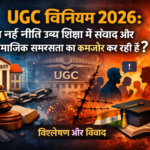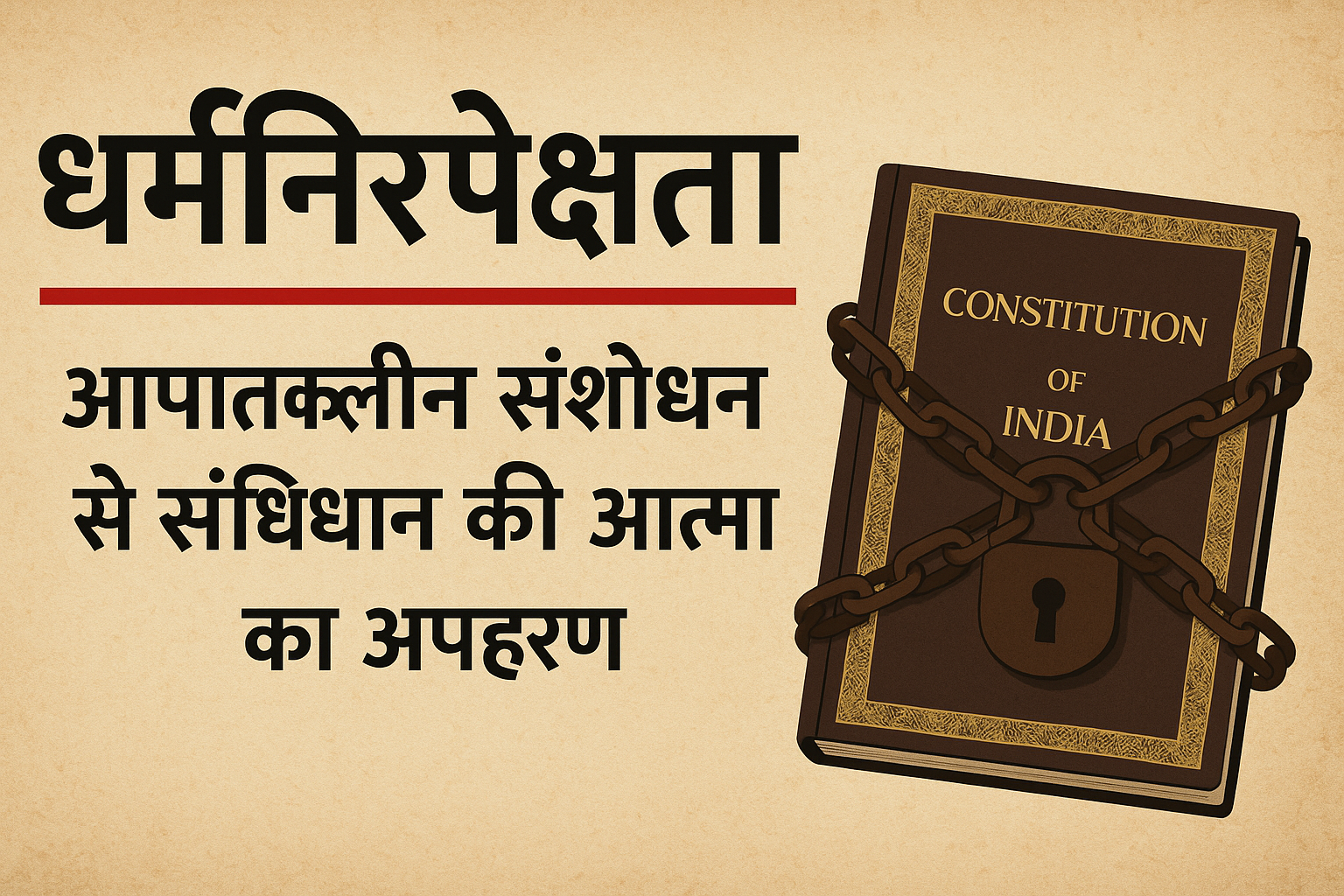
धर्मनिरपेक्षता: आपातकालीन संशोधन से संविधान की आत्मा का अपहरण
25 जून को देश में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। कई विद्वानों ने कहा कि “धर्मनिरपेक्षता” और “समाजवाद” जैसे शब्द भारतीय संविधान में असंवैधानिक रूप से, आपातकाल जैसे दमनात्मक वातावरण में जोड़े गए थे, और अब समय आ गया है कि इन्हें हटाया जाए। यह सुझाव किसी राजनीतिक लाभ की दृष्टि से नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा के पुनर्स्थापन का आग्रह है।
भारत के संविधान में “धर्मनिरपेक्षता” और “समाजवाद” शब्द वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत उस समय जोड़े गए जब देश पर आपातकाल थोपा गया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला यह काल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, जहाँ प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, और विपक्ष की आवाज़ को पूरी तरह कुचल दिया गया था। यह संशोधन उस समय किया गया जब संसद और न्यायपालिका, दोनों पर सत्ताधारी नेतृत्व का कठोर नियंत्रण था। जनमत, जनसंवाद और विधायी विमर्श के बिना इन मूलभूत शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ना भारतीय संविधान की आत्मा के साथ छल था।
संविधान की प्रस्तावना को उसकी “आत्मा” कहा जाता है, क्योंकि यही वह संक्षिप्त घोषणा है जो भारत के संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और मूलभूत दर्शन को परिभाषित करती है। लेकिन जिस आत्मा की रक्षा पूरे संविधान का उद्देश्य है, उसी प्रस्तावना को आपातकाल की तानाशाही में, जब लोकतंत्र निलंबित था और विपक्षी नेता जेलों में बंद थे, मनमाने तरीके से परिवर्तित कर दिया गया। यह बदलाव न तो सार्वजनिक सहमति से आया, न ही किसी स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस का परिणाम था। जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ ही निष्क्रिय थीं, तब ऐसे संशोधन को संवैधानिक कैसे माना जा सकता है? यह निःसंदेह इंदिरा गांधी के वैचारिक वर्चस्व का प्रतीक है जिसने संविधान की आत्मा का अपहरण कर लिया।
इंदिरा गांधी का झुकाव वामपंथी सोवियत मॉडल की ओर था, जहाँ समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को सत्ता संरचना का मूल तत्व माना जाता था। इस विचारधारा के अनुरूप वामपंथी गुटों ने “धर्मनिरपेक्षता” को भारतीय संविधान की मूल पहचान बनाने का दबाव बनाया। यह एक सुविचारित रणनीति, धर्मनिरपेक्षता को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि वह भारत की बहुसंख्यक हिंदू संस्कृति को राजनीतिक और वैधानिक रूप से सीमित कर सके, जबकि अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित किए जाएँ। ध्यातव्य हो कि वामपंथियों ने आपातकाल में इंदिरा गाँधी की सहायता के साथ-साथ गुप्तचरी कर लोगों को जेल भिजवाने का कार्य भी किया।
यह शब्द समय के साथ एक राजनीतिक औजार बनता गया, विशेषकर मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए। यह शब्द एकतरफा नीतियों और निर्णयों की जननी बन गया है। हज सब्सिडी, शरिया आधारित पर्सनल लॉ बोर्ड की स्वायत्तता, मदरसों को विशेष संरक्षण, और धार्मिक संस्थानों के लिए पृथक वित्तीय नीतिया, इन सभी ने तथाकथित “धर्मनिरपेक्षता” को “चयनात्मक तुष्टिकरण” में बदल दिया। इस दौरान बहुसंख्यक हिंदू समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मांगों की निरंतर उपेक्षा की गई।
इस विचारधारा ने न केवल नीतिगत असंतुलन पैदा किया, बल्कि हिंदू संस्कृति और आस्थाओं को सार्वजनिक जीवन से हटा देने की कोशिश की। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, हिन्दू पर्वों के आयोजन में बाधाएँ, शिक्षा नीति में प्राचीन भारतीय ज्ञान की उपेक्षा, ये सभी घटनाएँ दर्शाती हैं कि “धर्मनिरपेक्षता” का प्रयोग वस्तुतः एक बहुसंख्यक विरोधी वैचारिक हथियार है।
डॉ. भीमराव आंबेडकर स्वयं इस बात के पक्षधर नहीं थे कि “धर्मनिरपेक्षता” शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया जाए। उनका मानना था कि यह भावना संविधान के ढांचे में अंतर्निहित है और इसे अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब संविधान अंगीकृत हुआ, तब भी “धर्मनिरपेक्षता” को शब्द रूप में सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि अनुच्छेद 14, 15, 25–28 पहले से ही धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दे रहे थे।
यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी राष्ट्रों की अवधारणा पर आधारित है, जहाँ चर्च और राज्य का पृथक्करण होता है। किंतु भारत में राज्य और धर्म का संबंध सदा से परस्पर सह-अस्तित्व का रहा है। यहाँ “राज्य” न किसी धर्म का द्रोही रहा, न पोषक। आज अनेक विचारक, समाज संगठन और राजनीतिक दल इस प्रश्न पर फिर से विमर्श कर रहे हैं कि क्या संविधान की प्रस्तावना को उस स्थिति में लौटाया जाए, जहाँ यह 26 जनवरी 1950 को था, जब भारत “पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” था, और उसकी आत्मा में सबके लिए समान स्थान था। संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है; यह एक जीवंत दस्तावेज है जो जनमानस की आकांक्षाओं, अनुभवों और समय की कसौटी पर खरा उतरता रहे, यही उसकी सफलता है।
अलोकतांत्रिक तरीके जोड़ा गया “धर्मनिरपेक्षता” शब्द का संविधान में बने रहना न केवल एक ऐतिहासिक त्रुटि है, बल्कि यह भारतीय अस्मिता पर वैचारिक बोझ जैसा बन गया है। यह शब्द आज भारतीय राजनीति में एक छद्मनैतिक आवरण बन चुका है, जो असल में वोटबैंक की राजनीति और सामाजिक विभाजन का कारक है।
यदि भारत को एक निष्पक्ष, समरस और न्यायपूर्ण राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है, तो अब समय आ गया है कि “धर्मनिरपेक्षता” शब्द को संविधान की प्रस्तावना से औपचारिक रूप से हटाया जाए। धर्मनिरपेक्षता को यदि वाकई बनाये रखना है, तो उसका अर्थ सभी पंथों के प्रति निष्पक्ष और समान व्यवहार होना चाहिए, ना कि केवल एक समुदाय के तुष्टिकरण और दूसरे के अधिकारों के हनन का औचित्य। लेकिन जब तक यह शब्द व्यवहार में भेदभाव और असंतुलन को बढ़ावा देता है, तब तक इसे हटाना ही संविधान के आत्मसम्मान और भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के अनुरूप है। यही वह वैचारिक निर्भीकता है, जिसकी आज लोकतांत्रिक भारत को सबसे अधिक आवश्यकता है। अब जब देश लोकतंत्र की हत्या के उस काले अध्याय का 50वां वर्षगांठ मना रहा है। विद्वतजनों और मीसा के काराबन्दियों से हमने इंदिरा सरकार की हिटलर से अधिक बर्बर तानाशाही की निर्मम घटनाएं सुनी तब हमें उस दौर में हुए संविधान संसोधन पर व्यपक चर्चा करनी चाहिए. इन पचास वर्षो में उन संसोधनों से देश पर क्या प्रभाव पड़े इस पर विचार करना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द पर जनमन को खुलेमन से चर्चा और चिंतन करने के लये प्रेरित करना चाहिए। यह भारत की आत्मा के पुनर्निर्माण की दिशा में एक आवश्यक और साहसिक कदम होगा।