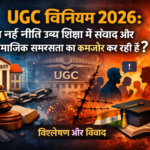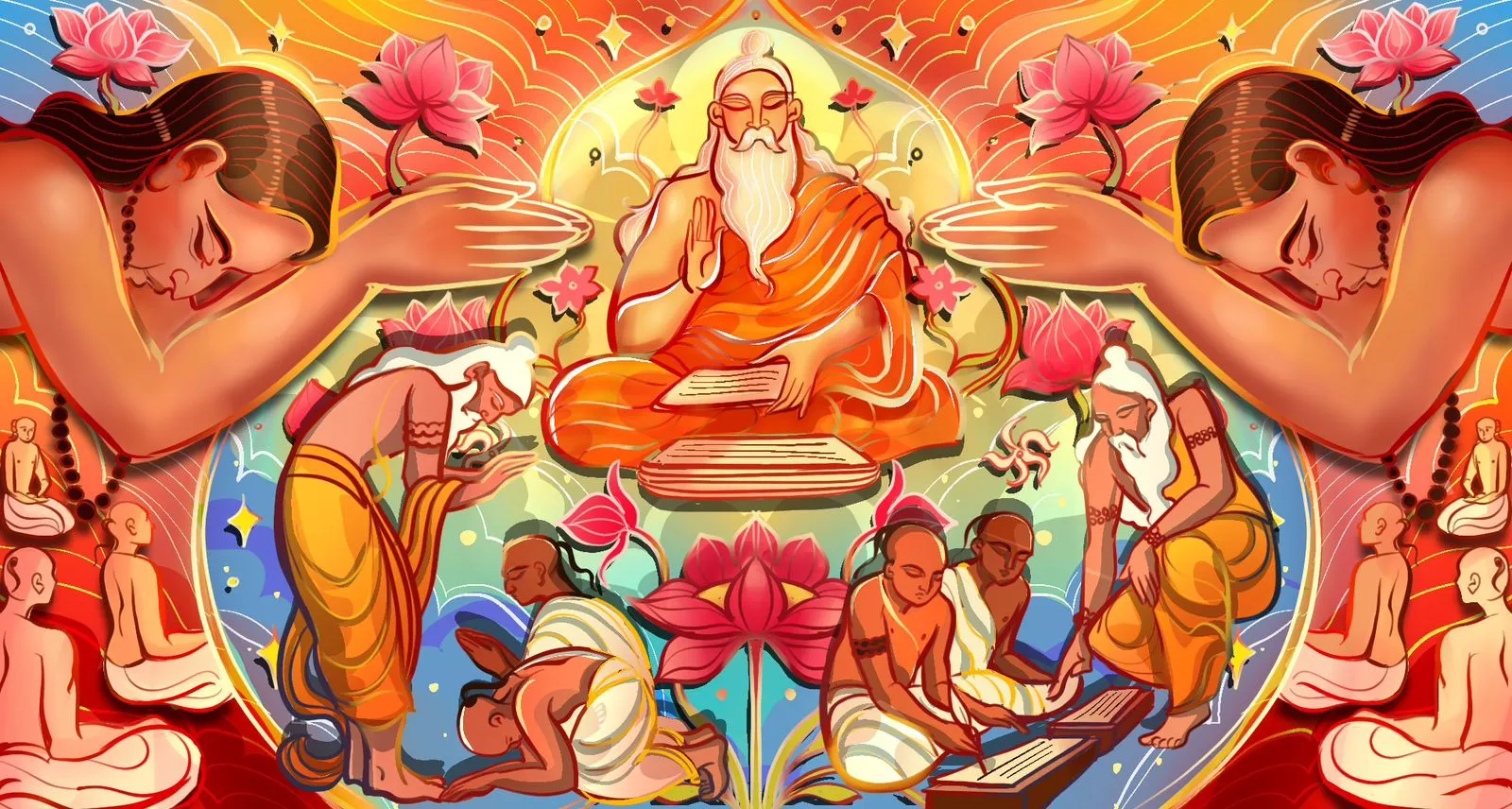
भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व: वेदव्यास, गुरु पूर्णिमा और विश्वगुरु भारत
भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व अपार है। हर एक प्रसिद्ध चरित्र का उदाहरण देखें तो वे सभी किसी न किसी को अपना गुरु मानते थे। जीवन में विकट स्थिति को पार करने के लिए उन्होंने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए ही सफलता प्राप्त की। अर्थात, गुरु पथ-प्रदर्शक हैं। शब्द का विश्लेषण करें तो ‘गु’ का अर्थ अंधकार और ‘रु’ का अर्थ प्रकाश है। अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश कर वे सही राह दिखाते हैं। इसीलिए कहा गया है—
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।।
अर्थात, अज्ञानता के अंधकार में अंधे हुए व्यक्ति की आँखें जो ज्ञान की अंजन शलाका से खोल देते हैं, उन्हें ही गुरु कहा गया है और हम उन्हें नमन करते हैं। वे सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं – भौतिक और अधिभौतिक अथवा आध्यात्मिक। इस चराचर जगत में कैसे चलना है, कैसा व्यवहार करना है, और साथ ही हमारे सांसारिक जगत से परे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है – ऐसे ही प्रश्नों का समाधान गुरु ही करते हैं। आत्मा और परमात्मा का बोध कराते हैं, उन्हें ही हमने गुरु माना है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है—
अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।।
अर्थात, अखण्ड मण्डलाकार विश्व-ब्रह्मांड के सभी चर और अचर में व्याप्त परमेश्वर का साक्षात्कार जो करवाते हैं, वे ही गुरु हैं और उन गुरु को नमन।
गुरु में ही ईश्वर के गुणों को हम देख पाते हैं। वे हमारे भीतर अच्छे गुणों का सृजन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं तथा अवगुणों का नाश करते हैं। और हमें ब्रह्म के स्वरूप से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में मान दिया गया है, और साथ ही उन्हें परब्रह्म का स्वरूप मान कर हम वंदन करते हैं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परंब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥
मनुष्य जीवन में प्रथम गुरु तो माता ही हैं, जिन्होंने हमें जगत से परिचित कराया। चलना, बोलना, उचित-अनुचित का भेद समझाया। दूसरा गुरु पिता हैं, जिन्होंने हमें समाज के बाह्य रूप से परिचित कराया। उसी प्रकार आत्मीय-सुहृद भी कई प्रकार का ज्ञान कराते हैं। परन्तु इससे अतिरिक्त, अपने गुणों का विकास कराने वाला, जीवन का ज्ञान देने वाला, सत्य का मार्ग दिखाने वाला, आत्मा-परमात्मा का ज्ञान देने वाला शिक्षा गुरु होता है। अध्यात्म की ओर ले जाने वाला दीक्षा गुरु भी होता है।
गुरु हमारे लिए माता, पिता, सुहृद तथा मित्र भी होते हैं। गुरु हमें माता के जैसे स्नेहपूर्वक, पिता के जैसे कठोर शासन के साथ, सुहृद या आत्मीय के जैसे परामर्श के माध्यम से और मित्र के जैसे सरलतापूर्वक शिक्षा देते हैं। दूसरी ओर देखें तो माता, पिता, सुहृद और मित्र – ये सभी कई स्थितियों में गुरु के रूप में सामने आकर हमें सही मार्गदर्शन कराते हैं।
गुरु का स्थान भारतीय समाज तथा संस्कृति में अत्यंत उच्च है। गुरु के साथ व्यक्ति का संबंध शिष्य का होता है। गुरु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य बनना पड़ता है। बिना शिष्य-भाव के यह ज्ञान समझना असंभव है। भारतीय चातुराश्रम व्यवस्था के अनुसार, व्यक्ति जीवन के चार अध्याय होते हैं, जिसमें प्रथम अध्याय है ब्रह्मचर्य। शिशु का उपनयन तथा विद्यारंभ संस्कार के उपरांत विद्या अर्जन हेतु वह गुरु गृह या आश्रम में जाकर सभी भौतिक सुख-सुविधाओं से दूर रहते हुए गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए शिक्षा प्राप्त करता था। वेद-अभ्यास के साथ-साथ भौतिक विषयों की शिक्षा, व्यक्ति जीवन, कर्म जीवन, समाज जीवन, राज्य, राजनीति आदि सभी विषयों पर शिक्षा प्राप्त की जाती थी।
गुरु परंपरा केवल मनुष्य जीवन में ही है, ऐसा नहीं। देवताओं तथा दानवों के भी गुरु होते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य हैं। मानवों के लिए व्यक्तिगत तथा कुल गुरु और राज्यों में राजगुरु होने का विषय हम सभी जानते हैं।
परन्तु आदि गुरु के रूप में महर्षि वेदव्यास जी का हम सभी आदर करते हैं, और उन्हीं के जन्म तिथि को देश तथा विश्व भर में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। कृष्ण वर्ण के कारण उनका नाम पड़ा कृष्ण, द्वीप में जन्म होने के कारण द्वैपायन, तथा अपनी उच्चतम ज्ञान-शक्ति से वेदों को चार भागों में विभाजित करने के कारण उनका नाम पड़ा वेदव्यास।
आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भारतीय परंपराओं को मानने वाले सभी अपने गुरु को गुरु वेदव्यास के प्रतिरूप मानकर, व्यासासन में गुरु को या उनके चित्र को रखकर पूजन करते हैं और दक्षिणा समर्पण करते हैं। कुछ लोग प्रतीक को ही गुरु मानकर पूजन करते हैं।
हमारे शास्त्रों में अवधूत दत्तात्रेय का एक उदाहरण मिलता है, जिनके चौबीस गुरु थे। पृथ्वी: क्षमा, परोपकार, सहनशीलता और स्थिरता का प्रतीक। जल: स्वच्छता और मधुरता का प्रतीक। अग्नि: ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक। वायु: गतिशीलता और परिवर्तनशीलता का प्रतीक। आकाश: विशालता और असीमत्व का प्रतीक। ऐसे ही जिन-जिन से भी उन्हें गुणों की प्राप्ति हुई, प्रत्येक को उन्होंने गुरु माना।
उनके अन्य गुरु थे – चंद्रमा, सूर्य, कपोत (कबूतर), अजगर, समुद्र, पतंगा, भ्रमर, मधुमक्खी, गज (हाथी), हिरण, मछली, पिंगला वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, सर्प, बाण बनाने वाला, मकड़ी और भृंगी।
महाभारत में एकलव्य का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित कर उनसे ही शिक्षा प्राप्त कर ली।
भारतीय परंपराओं में सिख समुदाय ने दस व्यक्तित्व गुरु के पश्चात गुरु ज्ञान के संग्रह ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना।
भारत के स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी प्रतीकात्मक गुरु के रूप में परम पवित्र भगवा ध्वज को ही गुरु रूप में ग्रहण किया है।
अर्थात, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकें, सही मार्गदर्शन पा सकें, वे किसी भी रूप में हों, गुरु हैं। यदि मन में शिष्यत्व का भाव हो, तो उसी गुरु से पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
भगवा ध्वज भी भारतीय परंपराओं का अभिन्न अंग है। यह चारों युगों में विद्यमान तथा पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। देवासुर संग्राम से लेकर आज तक के युद्धों में इसे धर्म ध्वज, राज्य ध्वज के रूप में मान दिया जाता था। भगवान श्रीराम का अरुण ध्वज, श्रीकृष्ण का कपिध्वज, दोनों ही भगवा ध्वज थे।
इस रंग की अपनी अनोखी विशेषता है – सूर्योदय के समय प्रकाश का रंग, यज्ञों में उठती अग्नि शिखा का रंग ही भगवा है। इसी अग्निवर्ण के वस्त्र को धारण कर व्यक्ति संन्यास लेकर भौतिक सुख का परित्याग कर राष्ट्र, धर्म तथा समाज हित में अपना जीवन समर्पित करता है, अथवा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने लगता है।
ऐसे ही ज्ञान-गंगा के प्रवाह को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कई गुरु भारत तथा विश्व की यात्रा पर निकले। आदि शंकराचार्य भारत के चारों दिशाओं में प्रवास कर चारों प्रमुख स्थानों पर मठों की स्थापना किए।
इसी प्रकार माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निंबार्काचार्य जैसे कई गुरु शास्त्र ज्ञान को लेकर आगे बढ़े।
गुरु नानकदेव जी ने भजन-कीर्तन के माध्यम से सरलतापूर्वक सामान्य जनजीवन में अध्यात्म का बोध कराया।
बंग प्रदेश के ठाकुर श्रीरामकृष्ण परमहंस ने कथा-कहानी और सरल बोलचाल के माध्यम से नास्तिकता के बड़े-बड़े दिग्गजों को भी ईश्वर का महत्व अनुभव करवाया।
समर्थ स्वामी रामदास ने अध्यात्म ज्ञान के साथ-साथ भारत की सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज से हिन्दवी स्वराज्य का निर्माण करवाया।
भारत के दक्षिण में गुरु विद्यारण्य स्वामी ने हरिहर और बुक्का से धर्म राज्य की स्थापना करवाई।
भगवान बुद्ध ऐसे गुरु थे, जो अपने शिष्यों से कहते थे – “आत्मदीपो भव।” अर्थात, अपने भीतर के ज्ञान के प्रकाश से अपना रास्ता स्वयं बनाओ।
गुरु कृपा तभी प्राप्त हो सकती है जब गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण हो। गुरु के बताए मार्ग पर निःसंदेह होकर, गुरु ज्ञान को पाथेय बनाकर चलें, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्।
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षयम्॥
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम्।
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा॥
गुरु और शिष्य के बीच वार्ता का अनुपम श्लोक हमें वेद से प्राप्त होता है—
ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवाव है।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
अर्थ: हम शिष्य और शिक्षक साथ आगे चलें, हम दोनों साथ विद्या के फल का भोग करें, हमारा किया हुआ अध्ययन प्रभावशाली हो, हम एक-दूसरे की शक्ति बनें और हमारे बीच परस्पर द्वेष न हो। हमारा वातावरण तथा मन शांत और निर्मल रहे।
सिद्ध योगी गोरक्षनाथ की गुरु भक्ति जन-जन में प्रसिद्ध है। उन्होंने गुरु के लिए अपनी आँखें तक त्याग दी थीं। उपमन्यु और आरुणि की गुरु आज्ञा पालन की कथाएँ सभी को ज्ञात हैं।
हम किसी भी शिक्षक को गुरु कह देते हैं, परंतु जो केवल उचित ज्ञान देते हैं, वही सच्चे अर्थों में गुरु हैं। उचित ज्ञान क्या है? इसका उत्तर महर्षि वेदव्यास जी के एक प्रमुख श्लोक में वर्णित है—
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।
परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्॥
अर्थात, अठारह पुराणों का सार महर्षि ने दो वचनों में निहित किया है – परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है।
सभी गुरु इसी शाश्वत ज्ञान को ही अपने शिष्यों को बताते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है – सेवा ही परम धर्म, यत्र जीव तत्र शिव, अतिथि देवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा।
यह ज्ञान विश्व को देने के लिए ही उद्घोष हुआ – “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्।”
भारत ने विश्व को कभी पराया नहीं माना, उसे अपना कुटुंब माना। तभी तो भारत ने कहा – “वसुधैव कुटुम्बकम्।”
भारत की गुरु परंपरा उसी ज्ञान-गंगा को प्रवाहित कर रही है। भारत सदैव सबका कल्याण करता आ रहा है, क्योंकि भारत उसी महान शिक्षा का धारक, वाहक तथा संरक्षक है।
सभ्यता और संस्कृति में भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु था, और आगे चलकर भारत पुनः विश्व गुरु बनकर कल्याण और शांति का मार्ग दिखाएगा।